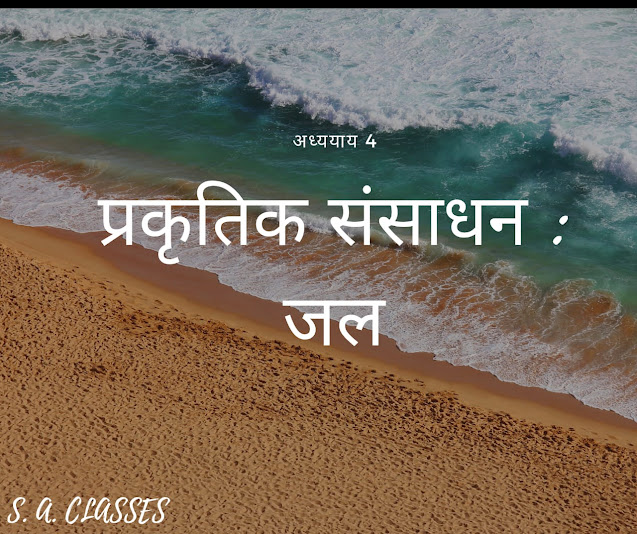
प्रकृतिक संसाधन : जल
WATER RESOURCE
अध्याय 4 : संसाधन
‘जल ही जीवन है’।
पृथ्वी पर जल का होना ही उसे अन्य ग्रहों की अपेक्षा विशेष महत्व प्रदान करता है।
हमारी पृथ्वी प्रायः 'जलीय ग्रह'/ नीला ग्रह ( Blue Planet) कही जाती है क्योंकि भूपृष्ठ का अधिकतर भाग महासागरों से अच्छादित
है। वाष्पीकरण, संघनन, और
वर्षण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से ही हम अपना सारा मीठा या ताजा जल प्राप्त करते
हैं। भारत में ताजे जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई की सुविधाएँ प्रदान करने में
होता है जिससे खेतों से अधिक से अधिक पैदावार ली जाती है।
जल राष्ट्रीय संसाधन है जो दो प्रकार के
होते है – (i)
मीठा जल और (ii)
खारा जल
जल के स्रोत
जल जीवों की उत्पत्ति का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल-स्रोंत विविध रूपों में पाये जाते हैं।
1.
भू-पृष्ठीय जल 2. भूमिगत जल, तथा 3. वायुमंडलीय जल 4. महासागरीय जल
जीवन में भू-पृष्ठीय और
भूमिगत जल का ही प्रत्यक्षतः उपयोग होता हैं। अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन इस
प्रकार है
1. भू-पृष्ठीय जल : धरातल पर पाये जाने वाले जल भू-पृष्ठीय या
धरातलीय जल कहलाते हैं। जिसका अधिकांश भाग नदी-नालों, झील-तालाबों तथा ताल-तलैया में तथा शेष जल सागर एवं महासागरों में
पाये जाते है। भू-पृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। वर्षण का लगभग 20 प्रतिशत भाग
वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं।
2. भूमिगत जल : वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस-रिस कर कठोर
शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है । अर्थात्, विभिन्न माध्यम से जल रिसकर बड़े- प्रक्रिया से एकत्रित जल ‘भौम जल’ के नाम से भी जाना जाता है।
जल: कुछ रोचक तथ्य:
1.पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% समुद्र और सागरों में पाया जाता है।
2. पूरे जल का लगभग 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है।
कुल ताजे पानी का 70%
आइसबर्ग और ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ के रूप में मौजूद है।
3.कुल ताजे पानी का 30%
से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित है।
४.पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है।
प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल
की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133 वाँ स्थान
है।
5.भारत में पुन:चक्रीकरण के
लायक जल संसाधन 1,897 वर्ग किमी प्रति वर्ष है।
6.ऐसा अनुमान है कि 2025
तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जायेगा जहाँ पानी की भारी कमी
है।
भारत में जल के स्रोत-उनका वितरण और उपयोग
जल संसाधन के रूप में समान रूप से वितरित नहीं है। हमारे देश में
इसके मुख्य स्रोत निम्नांकित हैं-
वर्षा: भारत में औसतन 118 सेमी.
वर्षा होती है। भारत के जल संसाधनों का एक बड़ा अनुपात उन क्षेत्रों में है, जहां औसतन 100 सेमी.
वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा भूमिगत जलभूतों के पुनर्भरण को मुख्य साधन भी है।
भूमिगत जल- इसे कुआं खोद कर निकाला जाता है । इसके लिए भी वर्षा एक प्रमुख साधन है। जहाँ
वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ
गहरे कुएँ खोदने पड़ते हैं और उनका जल प्राय: खारा होता है, जैसे राजस्थान में । भूमिगत जल (अंतर्भौम जल) का अधिक उपयोग उत्तर
भारत में ही हो पाता है। अब तक हम 37% भूमिगत जल का प्रयोग करने में समर्थ हुए
हैं। भारत में लगभग 433 अरब घन मीटर भूमिगत जल है। इसका 42 प्रतिशत केवल उत्तरी
मैदान में है। इसमें 19 प्रतिशत जल अकेले उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में प्रचुर मात्रा में भूमिगत
जल विद्यमान है।
नदियाँ- अब तक हम नदियों कुल
प्रवाहित जल का के मात्र 8.5% ही सिंचाई और विद्युत-उत्पादन में उपयोग कर सके हैं, शेष 91.5% जल बहकर समुद्र में चला जाता है । भारतीय नदियों का औसत
जल-बहाव (वर्षभर में) 1,869 अरब घनमीटर है।
झील, तालाब एवं अन्य जलाशय- देश के विभिन्न भागों
में ये पाए जाते हैं। इनका जल भी उपयोग में लाया जाता है। तालाबों की अधिक संख्या
दक्षिण भारत में (पठारी भाग में) है।
ग्लेशियर- गर्मी में पिघलकर ये
नदियों को जल प्रदान करते हैं। भारत में इनका क्षेत्र उच्च हिमालय है। हिमालय की चोटियाँ
हिमाच्छादित हैं और वे पिघलकर नदियों को जलपूरित रखती हैं। दक्षिण भारत में
ग्लेशियर नहीं मिलते।
बहुउद्देशीय परियोजना
: उदेश्य, लाभ
एवं हानि
एक नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई उद्देष्यों जैसे-सिंचाई,बाढ़ नियन्त्रण, जल
एवं मृदा संरक्षण,जल
विद्युत, जल परिवहन,पर्यटन
का विकास ,मत्स्यपालन,कृषि
एवं औद्योगिक
विकास आदि की पूर्ति करती हैं;बहुउद्देशीय परियोजनायें कहलाती हैं। जैसे-सतलज-ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना
जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों
के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुड परियोजना, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर,कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर,चेनाव
नदी पर सेलाल प्रोजेक्ट व भागीरथी नदी पर टिहरी बॉंध परियोजना।
बहुउद्देशीय परियोजना के उदेश्य
![]() 1.कृषि हेतु सिचाई सुविधा उपलब्ध बाढ़ पर नियन्त्रण करना
1.कृषि हेतु सिचाई सुविधा उपलब्ध बाढ़ पर नियन्त्रण करना
![]() 2.जल-विद्युत का उत्पादन करना
2.जल-विद्युत का उत्पादन करना
![]() 3.भूमि अपरदन पर प्रभावी नियन्त्रण करना
3.भूमि अपरदन पर प्रभावी नियन्त्रण करना
![]() 4.उद्योग-धन्धों का विकास करना
4.उद्योग-धन्धों का विकास करना
![]() 5.मत्स्य पालन का विकास करना
5.मत्स्य पालन का विकास करना
![]() 6.जल परिवहन का विकास करना
6.जल परिवहन का विकास करना
![]() 7.शुद्व पेयजल की व्यवस्था
करना
7.शुद्व पेयजल की व्यवस्था
करना
बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ
![]() 1.बॉंधों में एकत्रित जल का
प्रयोग सिंचाई के लिये किया जाता है।
1.बॉंधों में एकत्रित जल का
प्रयोग सिंचाई के लिये किया जाता है।
![]() 2. ये जल विद्युत ऊर्जा
प्राप्ति का प्रमुख साधन है।
2. ये जल विद्युत ऊर्जा
प्राप्ति का प्रमुख साधन है।
![]() 3. जल उपलब्धता के कारण जल की
कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगायी जा सकती हैं।
3. जल उपलब्धता के कारण जल की
कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगायी जा सकती हैं।
![]() 4.घरेलू व औद्योगिक कार्यों
में उपयोगी होता है।
4.घरेलू व औद्योगिक कार्यों
में उपयोगी होता है।
![]() 5.बाढ़ नियंत्रण,मनोरंजन,यांत्रिक नौकायन,मत्स्य
पालन व मृदा संरक्षण में सहायक हैं।
5.बाढ़ नियंत्रण,मनोरंजन,यांत्रिक नौकायन,मत्स्य
पालन व मृदा संरक्षण में सहायक हैं।
बहुउद्देशीय परियोजना से हानि
![]() 1.नदियों का प्राकृतिक बहाव
अवरुद्ध होने से तलछट बहाव कम हो जाता है।
1.नदियों का प्राकृतिक बहाव
अवरुद्ध होने से तलछट बहाव कम हो जाता है।
![]() 2. अत्यधिक तलछट जलाशय की तली
पर जमा हो जाता है।
2. अत्यधिक तलछट जलाशय की तली
पर जमा हो जाता है।
![]() 3.इससे भूमि का निम्नीकरण होता
है।
3.इससे भूमि का निम्नीकरण होता
है।
![]() 4.भूकंप की संभावना बढ़ जाती
है।
4.भूकंप की संभावना बढ़ जाती
है।
![]() 5.किसी कारणवश बॉंध के टूटने
पर बाढ़ आ जाना।
5.किसी कारणवश बॉंध के टूटने
पर बाढ़ आ जाना।
![]() 6.जलजनित बीमारियॉं,प्रदूषण,वनों की कटाई,
6.जलजनित बीमारियॉं,प्रदूषण,वनों की कटाई,
7. मृदा व वनस्पति का अपघटन हो
जाता है।
प्रश्न:3 बहुउद्देशीय
परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें।
उत्तर: बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले
लाभ और हानि निम्नलिखित हैं:
|
लाभ |
हानि |
|
बाढ़ नियंत्रण में मदद |
भारी संख्या में लोगों का विस्थापन |
|
जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल मिलता है। |
आजीविका की कमी |
|
अधिक से अधिक लोगों को पीने का पानी मिल पाता है। |
एक बड़ा भूभाग डूब जाता है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। |
|
बिजली का निर्माण होता है। |

भारत में शीर्ष 5 सबसे बड़े बांध
![]() टिहरी बांध, उत्तराखंड यह भारत का सबसे ऊँचा बांध ,
260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
टिहरी बांध, उत्तराखंड यह भारत का सबसे ऊँचा बांध ,
260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
![]() भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश ...
भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश ...
![]() सरदार सरोवर बांध, गुजरात ...
सरदार सरोवर बांध, गुजरात ...
![]() हीराकुंड बांध, ओडिशा ...
हीराकुंड बांध, ओडिशा ...
![]() नागार्जुनसागर बांध, तेलंगाना
नागार्जुनसागर बांध, तेलंगाना
जल में प्राकृतिक या मानव जन्य कारणों से जल की गुणवत्ता में आने
वाले परिवर्तन जल प्रदूषण कहते हैं
जल संकट
स्वेडन के जल संसाधन विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार, यदि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 1.000 घन मीटर की दर से भी जल उपलब्ध न
हो तो इसे जलाभाव मानना चाहिए। वर्तमान समय में जलराशि का बड़ा भाग प्रदूषित हो चुका है, फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है । जिस अनुपात में जल
प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, यदि
यह वृद्धि यूँ ही जारी रही, तो
वह दिन दूर नहीं जब अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए ।
जल संकट के मुख्य कारण
(i) देश
के कई भागों में अपर्याप्त वर्षा होना
(ii) जनसंख्या-वृद्धि
से जल की माग बढ़ना
(iii) नकदी
फसलों की खेती में जल की अधिक खपत
(iv) बढ़ते
जीवन-स्तर के परिणामस्वरूप जल की खपत बढ़ना
(v) नलकूपों
से अधिक जल निकासी के फलस्वरूप भूमिगत जल में कमी
जल संरक्षण का अर्थ
जल संरक्षण का अर्थ पानी बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। जल
संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि वर्षाजल हर समय उपलब्ध नहीं रहता अतः
पानी की कमी को पूरा करने के लिये पानी का संरक्षण आवश्यक है।
जल संरक्षण के लिये हर
स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। यदि निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए तो जल
संरक्षण सुगम हो जाता है।
1.
प्रत्येक गाँव/बस्ती में एक
तालाब होना आवश्यक है जिसमें जल संग्रह हो सके तथा आवश्यकतानुसार उपयोग में लाया जा
सके।
2.
नदियों पर छोटे-छोटे बाँध व
जलाशय बनाए जाएँ ताकि बाँध में पानी एकत्र हो सके तथा आवश्यकतानुसार उपयोग में
लाया जा सके
3.
3. नदियों में प्रदूषित जल को डालने से पूर्व उसे
साफ करना जरूरी है ताकि नदियों का जल साफ सुथरा बना रहे।
4.
अधिक से
अधिक वृक्षारोपण किया जाए ताकि ये वृक्ष एक तरफ तो पर्यावरण को नमी पहुँचाए तथा
दूसरी ओर वर्षा करने में सहायता करें।
5.
जल प्रवाह
की समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक है। कस्बों, नगरों से गंदे
पानी का निकास आवश्यक है।
6.
जल को व्यर्थ में बर्बाद न
करें और न ही प्रदूषित करें।
7.
भूमिगत जल का उपयोग समय तथा
उपलब्धता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ताकि आवश्यकता के समय इसका उपयोग किया जा
सके।
8.
भवनों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों में जल संरक्षण के
लिये व्यवस्था की जाए।
9.
जल को गहरी जमीन में छोड़ दें
ताकि वह अंदर जाकर भूजल स्तर को ऊपर उठाने में मदद करें।
10.
जल संरक्षण के लिये जल का
उचित संचय आवश्यक है।
11.
जल का उचित संवहन तथा
स्थानांतरण भी जल संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
12.
रेनवाटर हार्वेस्टिंग द्वारा
जल का संचयन।
13.
वर्षा जल को सतह पर संग्रहीत
करने के लिये टैंकों, तालाबों और चेक-डैम आदि की व्यवस्था।
14.
जल प्रबंधन का अर्थ
जल प्रबंधन का आशय जल संसाधनों के स्दुपयोग से है और जल की लगातार
बढ़ती मांग के कारण देशभर में जल के उचित प्रबंधन की आवश्यकता कई वर्षों से महसूस
की जा रही है। जल प्रबंधन के तहत पानी से संबंधित जोखिमों जैसे- बाढ़, सूखा और संदूषण आदि के प्रबंधन को भी शामिल किया जाता है।
देश में जल संरक्षण पर बल देना आवश्यक है और कोई भी इकाई (चाहे वह
व्यक्ति हो या कोई कंपनी) अनावश्यक रूप से उपकरणों के प्रयोग को कम कर रोज़ाना कई
गैलन पानी बचा सकता है।
प्रश्न- बाँध किसे कहते हैं? बाँधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता हैं?
उत्तर- बाँध एक अवरोध है जो जल को
बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से तो रुकती
ही जमा किये गया जल सिंचाई, जल
विद्युत, पेय जल की आपूर्ति, नौवहन
आदि में भी सहायक संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर किया जाता है।
बाधों को लकड़ी के बांध, पक्का
बांध तटबंध बांध के वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
प्रश्न:1राजस्थान
के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर: राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण निम्न
तरीकों से किया जाता है: लोग अपने घरों में टंका बनवाते हैं। इनमें वर्षा जल का
संग्रहण किया जाता है ताकि गर्मी के मौसम में उसका इस्तेमाल किया जा सके। कई जगहों
पर आज भी पुरानी बावलियों को साफ रखा जाता है। इनमें वर्षा जल का संग्रहण किया
जाता है ताकि गर्मी के मौसम में उसका इस्तेमाल किया जा सके।
प्रश्न:2 परंपरागत
वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षण एवं भंडारण
किस प्रकार किया जा रहा है।
उत्तर:आधुनिक काल में छत वर्षा जल संग्रहण काफी लोकप्रिय हो रहा
है। छत की नालियों को जमीन पर या जमीन के नीचे रखी टंकी से जोड़ा जाता है। इससे
वर्षा का जल नालियों द्वारा टंकियों में जमा होता है। टंकी के जल को परिष्कृत करने
का बाद इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग टंकी के जल को जमीन में रिसने देते हैं
ताकि भौमजल का नवीकरण हो सके। इस तरह से सालों भर जल की उपलब्धता बनाए रखने में
मदद मिलती है।
राष्ट्रीय जल नीति
क्या है?
UPDATES
नीति आयोग के अनुसार, भारत पहली बार जल संकट का सामना कर रहा है, यदि उपचारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2030 तक देश में पीने योग्य जल की कमी हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार नई राष्ट्रीय जल नीति (New Water Policy- NWP) के साथ ही जल से जुड़ी शासन की संरचना और नियामक ढाँचे में महत्त्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रही है। किंतु इन परिवर्तनों के लिये राज्यों के बीच आम सहमति बनाना बेहद जरूरी है। ज्ञातव्य है कि भारत की पहली जल नीति वर्ष 1987 में आई थी, जिसे वर्ष 2002 एवं 2012 में संशोधित किया गया था।
समाप्त
हमसे जुड़े











0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें